लोकतंत्र का महत्व, लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत, लोकतंत्र का अर्थ (loktantra kya hai, loktantra kise kahate hain, loktantra meaning, loktantra ke prakar)
जय हिन्द दोस्तों, जय हिन्द दोस्तों, दोस्तों क्या आप जानते हैं की लोकतंत्र क्या है? (What is democracy in Hindi).
अगर नहीं जानते तो आज हम आपको लोकतंत्र के बारे में (About Democracy in Hindi) बताने वाले हैं, दोस्तों आज हम आपको लोकतंत्र से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। तो इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ियेगा।
दोस्तों, लोकतंत्र शब्द बोलने में जितना छोटा है लेकिन इसका अर्थ उतना ही बड़ा और जटिल है। डेमोक्रेटिक (Democratic) शब्द यूनानी भाषा के डेमोस (Demos) और कृतियां (Cratia) यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोग और शासन, शाब्दिक अर्थ में जनता का शासन।
लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह “जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है”। तो चलिए दोस्तों इस लेख के माध्यम से आज हम जानेंगे की लोकतंत्र क्या है (What is Democracy in Hindi) और लोकतंत्र के महत्व के बारे में।
Table of Contents
- लोकतंत्र क्या है? (What is Democracy in Hindi)
- लोकतंत्र के प्रकार (Types of Democracy in Hindi)
- लोकतंत्र के उद्देश्य
- लोकतंत्र का महत्व (Importance of Democracy)
- लोकतंत्र के गुण और विशेषताएं
- लोकतंत्र के दोष
- लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है? (Main Principles of Democracy in Hindi)
- लोकतंत्र क्यों आवश्यक है?
- लोकतंत्र के स्तंभ
- भारत में लोकतंत्र का इतिहास
- एक लोकतांत्रिक सरकार के फायदे और नुकसान
- FAQ
लोकतंत्र क्या है? (What is Democracy in Hindi)
लोकतन्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, “लोक + तन्त्र”। लोक का अर्थ है जनता तथा तन्त्र का अर्थ है शासन। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है।
यह समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था की प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करता है।लोकतंत्र के द्वारा नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है।
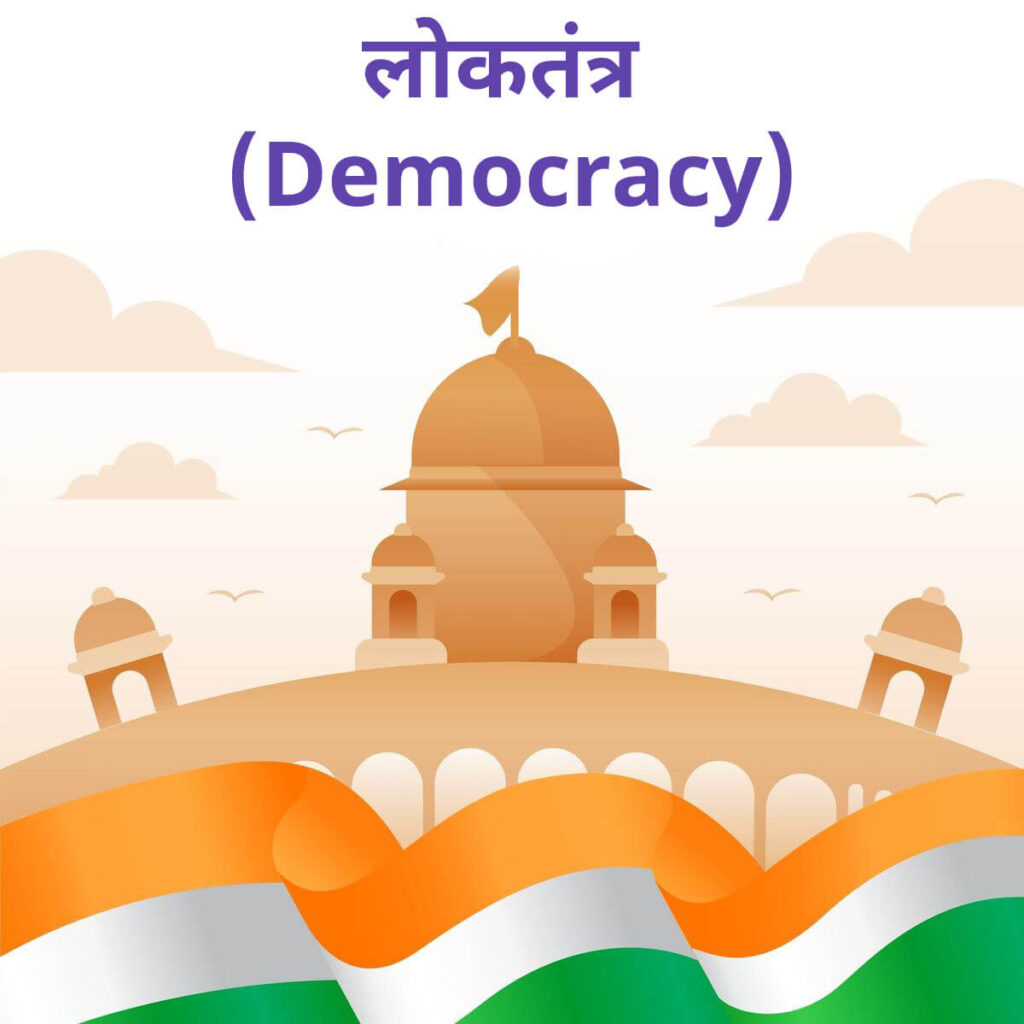
लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को समान रूप से मताधिकार प्रदान किए जाते हैं जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार निर्वाचित हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं।
अब्राहम लिंकन के कथनानुसार “लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है”। लोकतंत्र का राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय प्रणाली में भरपूर योगदान रहता है। यह देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कराती है।
लोकतंत्र के प्रकार (Types of Democracy in Hindi)
लोकतंत्र के प्रकार निम्नलिखित हैं –
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
- जनवादी लोकतंत्र
- समाजवादी लोकतंत्र
- विमर्श लोकतंत्र
- शास्त्रीय लोकतंत्र
- सहभागी लोकतंत्र
- ई लोकतंत्र
- प्रतिनिधि लोकतंत्र
प्रत्यक्ष लोकतंत्र
जब सामान्य जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है अर्थात नीति निर्माण का कार्य, उनका क्रियान्वयन एवं प्रशासन के अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यापक लोकतंत्र भी कहते हैं। जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं।
जनवादी लोकतंत्र
जनवादी लोकतंत्र का निर्माण साम्यवादी परंपरा के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत समाज में राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
इसकी स्थापना सर्वहारा क्रांति के पश्चात हुई थी जब सर्वहारा वर्ग के लोगों ने राजनीतिक निर्णय में अपनी भूमिका निभाना आरंभ किया था। जनवादी लोकतंत्र के माध्यम से समाज में साम्यवाद को बढ़ावा मिला था।
समाजवादी लोकतंत्र
दृष्टिकोण-लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है।
लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिसे स्वरूप पर बल देता है, उसे प्राय: लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है।
विमर्श लोकतंत्र
विमर्श लोकतंत्र के अंतर्गत सभी राजनीतिक कार्य एवं निर्णय नागरिकों की तर्कसंगत के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। विमर्श लोकतंत्र के अनुसार लोगों की सहमति से सभी सामाजिक नीतियों का निर्माण किया जाता है।
सहभागी लोकतंत्र
सहभागी लोकतंत्र का अर्थ है नीति निर्माण प्रक्रिया में जनसाधारण की भागीदारी। सहभागी लोकतंत्र आम जनता की ‘विशेषज्ञ’ के विरुद्ध प्रतिक्रिया है।
लोकतंत्र के सहभागितामूल्क सिद्धांत के अनुसार जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र का बुनियादी लक्षण है।
सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है।
ई लोकतंत्र
ई-डेमोक्रेसी (इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन), जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21 वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है।
यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। ई-लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है।
प्रतिनिधि लोकतंत्र
प्रतिनिधि लोकतंत्र वे लोकतंत्र हैं जिनमें लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों (चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से) के माध्यम से सरकार में भाग लेते हैं।
प्रतिनिधि मिलते हैं और पूरी आबादी के लिए निर्णय लेते हैं। इन लोकतंत्रों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। देश के सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है।
लोकतंत्र के उद्देश्य
- राज्य की संस्थाएं और संरचनाएं, राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, राजनीतिक शक्ति का आधार खुली प्रतियोगिता हो, व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण मिले।
- व्यक्तियों तथा विविध समूहों की व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी।
- राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक अधिकार आदि की गारंटी उपलब्ध कराई जाए।
- नीति-निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती की प्रक्रिया को अपनाना।
- राजनीतिक सहभागिता के लिए नियमन किया जाए।
- राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए।
लोकतंत्र का महत्व (Importance of Democracy)
लोकतंत्र के महत्व को दर्शाने के लिए निम्नलिखित तथ्य इस प्रकार हैं-
सत्ता के दुरूपयोग पर नियंत्रण
जहां सरकार होती है, वहां हमेशा सत्ता के दुरूपयोग का भय बना रहता है । इससे बचाव का एकमात्र तरीका यह है कि सत्ताधारी के हाथों में निस्सीम एवं निरंकुश सत्ता न सौंपी जाए, उस पर जनसाधारण का अंकुश और सार्थक नियंत्रण रहे।
लोकतंत्र की स्थापना इसी ध्येय को ध्यान में रखकर की जाती है।
शासन कार्य में जनसाधारण का सहयोग
लोकतंत्र में जनता की भागीदारी स्वीकार की जाती है क्योंकि इसमें प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसीलिए उन्हें जनजीवन के निकट आना होगा और जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय करने होंगे। इस प्रकार शासन में जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित होती है।
सार्वजनिक हित में कार्य
लोकतंत्र में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है । प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में कार्य करने के वादे के आधार पर चुनाव जीतते हैं।
दूसरे यह कि उन्हें पुनः चुनाव में प्रत्याशी बनना होता है, परिणामस्वरूप उन्हें सार्वजनिक हित के कार्यों को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
परस्पर सद्भावना और सम्मान का विस्तार
लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का पक्षपोषण नहीं किया जाता है। यह सभी के साथ समान व्यवहार करता है। इसमें व्यक्ति दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सीखता है।
जिससे उसका नैतिक स्तर ऊंचा होता है अर्थात् व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना और सम्मान बढता है, जिससे राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है।
देशभक्ति की भावना को बढावा
यह देशभक्ति की भावना को बढावा देता है । व्यक्ति के मन में जब यह विश्वास पैदा होता है कि देश में उसका अपना शासन है, तो देश के प्रति उसका प्रेम बढ जाता है। देश प्रेम से देश सुदृढ और सक्षम बनता है।
लोकतंत्र के गुण और विशेषताएं
- लोकतंत्र का सामान्य अर्थ उस राज्य अथवा सरकार से है जिसमें शासन की अंतिम सत्ता लोगों के हाथ में होती है जिसमें चुनाव का आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। लोकतंत्र में निश्चित समय पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को दोबारा चुनती है यदि जनता पुराने प्रतिनिधियों के कार्यों से असंतुष्ट है तो उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुन सकती है।
- लोकतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने भाषण देने लेख लिखने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता के अधिकार पर आधारित होती है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आधारित होती है नागरिकों के मौलिक अधिकारोें की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है।
- प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मत देने का अधिकार होता है किंतु सरकार का यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है कि सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते हैं।
- लोकतंत्र में स्वंतत्र व निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी जाती है।
- समाचार पत्रों को सरकार की नीतियों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की छूट होती है इस प्रकार यह जनता तथा सरकार के बीच कङी का काम करती है।
- लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना जाता है क्योंकि जनता ही अपने वोटो द्वारा निर्णय लेती है कि कौन सा दल सरकार बनाएगा।
- लोकतंत्र शासन पद्धति होने के साथ-साथ एक जीवन शैली भी है जिसमें सभी समूहों को अपने धर्म का पालन करने अपनी भाषा तथा संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
लोकतंत्र के दोष
- लोकतंत्र में शासन-व्यवस्था में अनावश्यक व्यय होता है।
- राजनीति को कमाई का पेशा बनाने की ओर झुकाव होता है।
- विधानसभाओं के सदस्यों तथा राजनीतिक अधिकारियों द्वारा कानून पास कराते समय वोटों को दृष्टि में रखना और समुचित व्यवस्था के भंग को सहन करना।
- लोकतन्त्र समानता व स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है। भारत में धर्म, भाषा और जाति ने राजनीति में प्रवेश पा लिया है और उसे दूषित भी कर रही है।
- भारत के संविधान के अनुसार यहाँ चुनावों की देखरेख, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व एक स्वाधीन व निष्पक्ष चुनाव आयोग पर है।
- समानता के सिद्धान्त का अपव्यय और प्रशासकीय पटुता या योग्यता के उचित मूल्य का न आंका जाना।
- भारत में शिक्षा का अभाव लोकतन्त्र का प्रमुख बाधक कारक है। अशिक्षित जनता अपने मत की उचित कीमत नहीं समझती। वे जाति या धर्म के आधार पर अपना वोट देते है।
- लोकतन्त्र की सफलता इस बार पर निर्भर होती है कि जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि योग्य और कुशल हों। परन्तु जब अयोग्य व्यक्ति केवल धन के बल पर चुनाव लङते है और जीतते हैं तो देश में लोकतन्त्र की प्रक्रिया रुक जाती है।
लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है? (Main Principles of Democracy in Hindi)
लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धांत
लोकतंत्र की उदारवादी परम्परा में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसी अवधारणाओं का प्रमुख स्थान रहा है।
लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत
बहुलवाद सत्ता को समाज में एक छोटे से समूह तक सीमित करने के बदले उसे प्रसारित और विकेन्द्रीकृत कर देता है।
लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धांत
इस सिद्धांत ने आम जनता की राजनीतिक कार्यों में भागीदारी को समर्थन किया जैसे – मतदान करना, राजनीतिक दलों की सदस्यता, चुनावों मे अभियान कार्य।
लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत
मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार भूमि, कल कारखाने इत्यादि पर जनता का स्वामित्व होता है। राज्य सारी प्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उत्पादन-क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर होते हैं।
लोकतंत्र क्यों आवश्यक है?
प्रत्येक व्यक्ति निर्बाध एवं स्वच्छंद जीवन जीना चाहता हैं। इसके लिए उसे आजादी चाहिए।
अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी, मन पसंद भाषा बोलने, खानपान और तीजत्यौहार मनाने की आजादी, धार्मिक नियमो का पालन करने की आजादी, देश के किसी भी भूभाग पर रहने, किसी भी व्यवसाय को चुनने एवं मनमाफिक जीवन जीने की आजादी को साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता हैं।
लोकतंत्र के द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए उसी सीमा मे सफ़ल होती हैं जहाँ नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता मे बाधक न बने।
इसके लिए संविधान मे नागरिक स्वतंत्रता के साथ ही मूलभूत कर्तव्यों का भी उल्लेख होता हैं।
यदि किसी राष्ट्र के संविधान द्वारा प्रदान की जाने वाली आजादी, राष्ट्र की एकता, संस्कृति एवं राष्ट्रीय मूल्यों के लिए ही खतरा बनने लगे, तो निश्चित ही इसके लिए कठोर संवैधानिक उपाय करने भी जरूरी हो जाते हैं।
लोकतंत्र के स्तंभ
लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं-
- विधायिका (Legislature)
- कार्यपालिका (Executive)
- न्यायपालिका (Judiciary)
- पत्रकारिता (Journalism)
विधायिका (Legislature)
आप सभी को यह बतादे की यह लोकतंत्र का पहला स्तम्भ होता है। इसका कार्य देश में कानून का बनाये रखना होता है। हमारे इस भारत देश में विधायिका का चुनाव हर पांच वर्षों में किया जाता है।
उसके बाद यह कुछ नियम व कानूनों का निर्माण भी करते है। इनके द्वारा बनाये गए नियमो को शाशक व प्रजा दोनों पर लागू होते है।
कार्यपालिका (Executive)
कार्यपालिका भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है। कार्यपालिका का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि कार्यपालिका ही विधायिका द्वारा बनाये गए सभी नियम व कानूनों को प्रजा तक पहुंचाने का कार्य करते है। उन सभी कानूनों को मानना व मनवाना भी इन्ही का कार्य होता है।
न्यायपालिका (Judiciary)
जैसा की हमने आप सभी को बताया है की लोकतंत्र के सभी स्तम्भ काफी महत्वपूर्ण होते है। इसलिए यह भी काफी आवश्यक होता है। क्योंकि न्यायपालिका लोगो को कानून को समझाने का कार्य करती है।
उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अगर कानूनों का उल्लंघन करता है। तो उस व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने की सजा भी देती है। केवल यह ही नहीं किसी भी व्यक्ति को इन्साफ यानि के न्याय दिलाने का कार्य भी न्यायपालिका का ही होता है।
पत्रकारिता (Journalism)
बाकी स्तंभों की ही तरह यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पत्रकारिता एक प्रकार से आम लोगो की आवाज के रूप से भी जानी जाती है।
पत्रकारिता का कार्य यह होता है की वह देश को लोगो को यह जानकारी प्रदान करें की देश में क्या चल रहा है। पत्रकारिता को किसी भी बारे में जनता को जानकारी खबर के माध्यम से पहुंचाने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है।
समय के साथ साथ पत्रकारिता में पहले के समय के मुकाबले काफी परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले के समय में पत्रकारिता समाचार पत्र के माध्यम से लोगो तक सही खबरे पहुंचाने का कार्य करती थी।
लेकिन आज के समय में पत्रकारिता लोगो को सही खबर प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुँचाती है।
भारत में लोकतंत्र का इतिहास
विश्व के विभिन्न राज्यों में राजतंत्र, श्रेणी तंत्र, अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र आदि शासन प्रणालियां प्रचलित रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आरंभ पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था।
प्राचीनकाल में भारत में सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण हैं।
वर्तमान संसद की तरह ही प्राचीन समय में परिषदों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती-जुलती थी। गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन इन्हीं परिषदों द्वारा होता था। इसके सदस्यों की संख्या विशाल थी।
उस समय के सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवि की केंद्रीय परिषद में 7,707 सदस्य थे वहीं यौधेय की केंद्रीय परिषद के 5,000 सदस्य थे। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों के अधिवेशन नियमित रूप से होते थे।
प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न जरूर थी।
सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है, परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है।
एक लोकतांत्रिक सरकार के फायदे और नुकसान
| लोकतंत्र के लाभ | लोकतंत्र के नुकसान |
| देश के लोग लोकतंत्र में सरकार का चुनाव करते हैं, इस प्रकार यह अंततः लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह होता है। | लोकतंत्र में सत्ता की कई परतें होती हैं, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया अन्य प्रकार की सरकार की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। |
| एक लोकतांत्रिक सरकार अपने लोगों को सरकार से ही सवाल करने के लिए और अधिक स्वतंत्रता देगी। उदाहरण के लिए, चीन के लोग सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि, भारत में लोकतंत्र लोगों को कुछ भी गलत होने पर सरकार से सवाल करने की अनुमति देगा। | एक लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार की संभावना होती है क्योंकि लोग चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है जहां लोग चुनाव के समय लोगों को पैसे देकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। |
| एक विपक्षी दल की अवधारणा है, इसलिए समय के साथ निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होगा। | भारत जैसे बड़े देश में हर पांच साल में राजनीतिक दलों के बदलाव के कारण विकास परियोजनाएं अस्थिर हो सकती हैं। |
FAQ
Q: लोकतंत्र किसे कहते हैं?
Ans: लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है।
Q: लोकतंत्र का अर्थ क्या है?
Ans: लोकतंत्र शब्द दो शब्दों लोक+तंत्र से बना है जिसका अर्थ है – लोगों का शासन।
Q: भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है?
Ans: भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है।
Q: लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी?
Ans: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी।
Q: अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
Ans: अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है।
Q: भारतीय प्रजातंत्र के जनक कौन है?
Ans: भारतीय प्रजातंत्र के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर हैं।
Q: लोकतंत्र के सिद्धांत बताइये?
Ans: स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व।
निष्कर्ष-
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा की लोकतंत्र क्या है? (What is democracy in Hindi) इसके अलावा आपको लोकतंत्र के बारे में (About Democracy in Hindi) बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमने आपको एक लोकतांत्रिक सरकार के फायदे और नुकसान भी बताया है।
साथ ही अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो, इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और उनको भी लोकतंत्र क्या है? (What is democracy in Hindi) लोकतंत्र के बारे में जानकारी दें। इस लेख को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द!